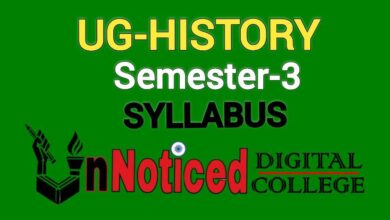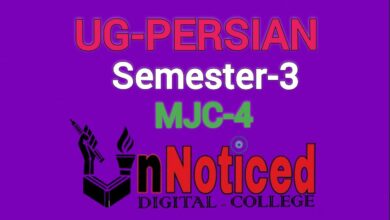2. यूरोप में पूर्णतंत्र (Absolutism)
पूर्णतंत्र, जिसे निरंकुश राजशाही भी कहा जाता है, एक राजनीतिक सिद्धांत और शासन का रूप था जिसमें एक सम्राट सर्वोच्च अधिकार रखता था और उसकी शक्तियाँ कानूनों, संविधान या रीति-रिवाजों से प्रतिबंधित नहीं होती थीं। यह शासन प्रणाली 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में प्रचलित थी और इस समय शासक अपनी शक्ति को केंद्रीकृत करते थे। इन शासकों ने अपने शासन को भगवान द्वारा प्रदत्त अधिकार (Divine Right) के सिद्धांत के माध्यम से न्यायसंगत ठहराया, जिसमें यह माना जाता था कि वे केवल ईश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं और इसलिए उनके पास अपने प्रजा पर पूर्ण अधिकार है। यूरोप में पूर्णतंत्र का युग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, जिसमें सम्राटों ने अपनी शक्तियों का लगभग अप्रतिबंधित उपयोग किया।
पूर्णतंत्र का उत्पत्ति
पूर्णतंत्र का उदय यूरोप में मध्यकालीन और पुनर्जागरण के प्रारंभिक समय में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक उथल-पुथल के कारण हुआ। इसके उत्पत्ति में कई कारण थे:
- फ्यूडलिज़्म का पतन: फ्यूडल सिस्टम, जो मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित था, 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान धीरे-धीरे समाप्त होने लगा। इसने सम्राटों को अपनी शक्ति को मजबूत करने और क्षेत्रीय नेताओं से अपनी सत्ता को केंद्रीकृत करने का अवसर दिया। फ्यूडलिज़्म का कमजोर होना राजाओं को सत्ता के एकमात्र स्रोत के रूप में स्थापित करने में मदद करता था।
- धार्मिक संघर्ष: 16वीं शताब्दी में हुई प्रोटेस्टेंट सुधार ने यूरोप में धार्मिक विखंडन पैदा किया। कैथोलिक चर्च की सत्ता को चुनौती मिली, और यूरोपीय राज्य धार्मिक आधार पर विभाजित हो गए। विशेष रूप से कैथोलिक देशों जैसे फ्रांस और स्पेन के शासकों ने अपनी सत्ता को एकजुट करने के लिए धर्म पर नियंत्रण किया।
- आर्थिक परिवर्तन: बाजार अर्थव्यवस्था के विकास, साथ ही विदेशी व्यापार और अन्वेषण से मिली समृद्धि ने सम्राटों को सैन्य बलों का विस्तार करने और अपनी केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान किए। इस समृद्धि ने उन्हें अन्य शक्तियों से स्वतंत्र बना दिया और उनके नियंत्रण को और अधिक मजबूत किया।
- पेशेवर सेना का उदय: खड़ा की गई स्थायी सेनाएँ, जो राज्य द्वारा वित्तपोषित थीं, सम्राटों को अपनी शक्तियों को बनाए रखने में सक्षम बनाती थीं। एक पेशेवर सेना, जो केवल सम्राट के प्रति वफादार थी, ने पूर्णतंत्र शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पूर्णतंत्र के लक्षण
पूर्णतंत्र के तहत शासक की शक्ति केंद्रित और बिना रोक-टोक के होती थी। कुछ मुख्य लक्षण थे, जो पूर्णतंत्र शासन को परिभाषित करते थे:
- शक्ति का केंद्रीकरण: पूर्णतंत्र की एक केंद्रीय विशेषता थी, शासक के हाथों में पूरी शक्ति का केंद्रीकरण। सम्राट या सम्राज्ञी राज्य के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखते थे, जैसे सैन्य, न्यायपालिका और प्रशासन। शासक ने अपने आसपास के शक्तियों को समाप्त कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि राज्य के सभी निर्णय केवल उनके नियंत्रण में हों।
- राजा का दिव्य अधिकार: सम्राटों ने अपनी शक्ति को दिव्य अधिकार (Divine Right of Kings) से वैध ठहराया, अर्थात यह विश्वास किया जाता था कि उनके पास शासन करने का अधिकार सीधे भगवान से आता है। इस सिद्धांत के तहत, सम्राट की सत्ता को चुनौती देना भगवान की इच्छा के खिलाफ माना जाता था। इस सिद्धांत का उपयोग सम्राटों ने अपनी पूर्ण शक्ति को उचित ठहराने के लिए किया।
- शक्ति पर कोई रोक-टोक नहीं: पूर्णतंत्र के तहत, सम्राट के पास अपनी शक्ति पर कोई रोक-टोक नहीं होती थी। कोई भी लोकतांत्रिक संस्थाएँ, जैसे संसद या प्रतिनिधि संस्थाएँ, सम्राट की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकती थीं। सम्राट सभी कानूनों, सैन्य कार्यों और विदेश नीति पर एकतरफा नियंत्रण रखते थे, और असहमति या विरोध को अक्सर दबा दिया जाता था।
- मजबूत नौकरशाही और स्थायी सेनाएँ: सम्राटों ने अपने राज्यों को चलाने के लिए एक मजबूत नौकरशाही बनाई। इन नौकरशाहों के प्रति सम्राट का वफादारी थी और वे सम्राट के आदेशों को लागू करने में मदद करते थे। स्थायी सेनाएँ, जो पेशेवर सैनिकों से बनी होती थीं, राज्य की सुरक्षा और सम्राट की सत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थीं।
- धर्म पर नियंत्रण: पूर्णतंत्र के शासक अपने क्षेत्रों में धर्म पर भी नियंत्रण रखते थे। कैथोलिक देशों में यह अक्सर सम्राट के धार्मिक संरक्षक के रूप में उनके भूमिका को स्थापित करने और धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार की रक्षा करने के रूप में होता था। प्रोटेस्टेंट देशों में भी, सम्राटों ने धार्मिक प्रथाओं पर नियंत्रण स्थापित किया और धार्मिक असहमति को दबाने की कोशिश की।
यूरोप में पूर्णतंत्र शासक
यूरोप के कई सम्राट पूर्णतंत्र शासन के प्रमुख उदाहरण थे। इनमें से कुछ प्रमुख सम्राटों में शामिल हैं:
- फ्रांस के लुई XIV (1643–1715): लुई XIV, जिसे “सूर्य सम्राट” (Sun King) के रूप में जाना जाता है, पूर्णतंत्र के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक थे। उन्होंने फ्रांस में सत्ता को केंद्रीकृत किया और प्रसिद्ध रूप से कहा, “L’État, c’est moi” (मैं ही राज्य हूं)। लुई XIV ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए नबियों की शक्ति को कम किया और सैन्य, अर्थव्यवस्था और चर्च पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया। उनका शानदार दरबार, जो वर्साय में स्थित था, उनके पूर्णतंत्र शासन का प्रतीक बन गया। हालांकि उनके शासनकाल में कला और संस्कृति में वृद्धि हुई, लेकिन उनकी महंगी युद्धों के कारण फ्रांस को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
- रूस के पीटर द ग्रेट (1682–1725): पीटर द ग्रेट एक परिवर्तनकारी शासक थे जिन्होंने रूस को आधुनिक बनाने और उसे एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बनाने की कोशिश की। उन्होंने राजनीतिक सत्ता को केंद्रीकृत किया, एक मजबूत सेना बनाई और रूस की समाजिक संरचना को यूरोपीय ढंग से सुधारने की कोशिश की। उन्होंने रूसी रूढ़िवादी चर्च पर भी नियंत्रण रखा और सैन्य विजय के माध्यम से रूस की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग शहर की नींव रखी, जो एक नई, सम्राट द्वारा नियंत्रित रूसी राजधानी बनी।
- प्रशिया के फ्रेडरिक द ग्रेट (1740–1786): फ्रेडरिक II, जिसे फ्रेडरिक द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, एक और पूर्णतंत्र शासक थे जिन्होंने प्रशिया में सत्ता को केंद्रीकृत किया। उन्होंने सैन्य विजय के माध्यम से प्रशिया का क्षेत्र बढ़ाया और अपनी नीतियों के माध्यम से “ज्ञानपूर्ण पूर्णतंत्र” की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जो पूर्णतंत्र शासन के साथ सुधारों का सम्मिलन था। उन्होंने कला और दर्शन के क्षेत्र में भी योगदान दिया, लेकिन उन्होंने राज्य के नियंत्रण को बनाए रखा।
- इंग्लैंड के चार्ल्स I (1625–1649): जबकि इंग्लैंड में कुछ समय के लिए पूर्णतंत्र शासक था, चार्ल्स I के शासन का अंत इंग्लिश नागरिक युद्ध और उनके निष्कासन में हुआ। चार्ल्स I ने दिव्य अधिकार के सिद्धांत को मानते हुए संसद के बिना शासन करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष और युद्ध हुआ। उनकी यह स्थिति असफल रही और उनकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड में संवैधानिक राजशाही की स्थापना हुई।
- स्पेन के फिलिप II (1556–1598): फिलिप II एक धार्मिक सम्राट थे जिन्होंने स्पेन में पूर्णतंत्र स्थापित किया। उन्होंने कैथोलिक धर्म की रक्षा की और यूरोप में प्रोटेस्टेंटवाद के खिलाफ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल स्पेन के साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन उनकी युद्धों और साम्राज्य की रख-रखाव के कारण स्पेन की अर्थव्यवस्था अंततः कमजोर हो गई।
पूर्णतंत्र का पतन
हालांकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में पूर्णतंत्र शासन का प्रभावी दौर था, लेकिन कई कारकों ने इसके पतन में योगदान किया:
- आर्थिक समस्याएँ: कई पूर्णतंत्र शासकों ने युद्धों, शानदार महलों और महंगी दरबारों पर भारी खर्च किया। इन खर्चों के कारण राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ गया, जिससे सम्राटों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, लुई XIV की युद्धों और खर्चों ने फ्रांस को वित्तीय संकट में डाल दिया।
- संसदीय शक्ति का उदय: इंग्लैंड जैसे देशों में, संसदीय शक्ति और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग ने धीरे-धीरे पूर्णतंत्र शासन को कमजोर कर दिया। 1688 में हुई ग्लोरियस क्रांति (Glorious Revolution) ने इंग्लैंड में संवैधानिक राजशाही की स्थापना की और पूर्णतंत्र का पतन हुआ।
- प्रकाशन युग (Enlightenment) के विचार: 18वीं शताब्दी में प्रकाशन युग ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा दिया। दार्शनिकों जैसे जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर ने पूर्णतंत्र और निरंकुश शक्ति के खिलाफ विचार प्रस्तुत किए। इन विचारों ने यूरोप के कई सम्राटों को प्रभावित किया और धीरे-धीरे पूर्णतंत्र के पतन में योगदान दिया।
- क्रांतियाँ: फ्रांसीसी क्रांति (1789) ने पूर्णतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पतन देखा। इस क्रांति ने बोरबॉन राजशाही को समाप्त किया और गणराज्य की स्थापना की। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे पूर्णतंत्र शासन को चुनौती मिली।
निष्कर्ष
यूरोप में पूर्णतंत्र एक ऐसा समय था जब सम्र
ाटों ने अपनी सत्ता को केंद्रीकृत किया और अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग किया। दिव्य अधिकार के सिद्धांत और मजबूत नौकरशाही ने सम्राटों को अपने राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी। हालांकि, युद्धों की आर्थिक समस्याएँ, प्रकाशन युग के विचार, और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग ने पूर्णतंत्र के पतन में योगदान किया। हालांकि पूर्णतंत्र ने यूरोप की राजनीतिक संरचना को आकार दिया, लेकिन स्वतंत्रता और संविधानिकता के विचारों ने नए प्रकार की शासन प्रणालियों को जन्म दिया, जिन्होंने यूरोप का भविष्य बदल दिया।
2. Absolutism in Europe
Absolutism, often referred to as absolute monarchy, was a political doctrine and form of government in which a monarch holds supreme authority, and his or her powers are not constrained by laws, constitutions, or customs. This system of governance was prevalent in Europe during the 16th, 17th, and 18th centuries and was marked by the centralization of power in the hands of the king or queen. Monarchs in this period justified their rule through the concept of divine right, asserting that they were appointed by God and thus had absolute power over their subjects. The era of absolutism in Europe significantly shaped the political, social, and economic landscape of the time, with monarchs exercising virtually unchecked authority.
Origins of Absolutism
The rise of absolutism can be traced back to the political instability and social turmoil in Europe during the late Middle Ages and the early Renaissance. Several factors contributed to the emergence of absolute monarchies:
- Decline of Feudalism: The feudal system, which had dominated medieval Europe, began to decline during the 15th and 16th centuries. The central authority of monarchs became stronger as feudal lords lost their power, and the monarchs centralized their rule. The decline of feudalism weakened the political power of regional nobles and allowed the monarchs to consolidate control.
- Religious Conflict: The Protestant Reformation, which began in the early 16th century, led to religious fragmentation in Europe. The Catholic Church’s authority was challenged, and various European states became divided along religious lines. Monarchs, particularly in Catholic countries like France and Spain, used their authority to control religious practices and unify their realms under their personal rule.
- Economic Changes: The growth of a market economy, combined with increased wealth from overseas exploration and trade, provided monarchs with the financial resources to expand their military forces and strengthen their central authority. This wealth allowed them to reduce their dependence on nobles and the church for funding, further centralizing power.
- Rise of Professional Armies: The development of standing armies, funded by the state, enabled monarchs to maintain control over their territories without relying on the feudal military system. A professional army, loyal directly to the king, was crucial in maintaining absolutist rule.
Characteristics of Absolutism
Absolutism was characterized by several defining features that consolidated the monarch’s control over state affairs:
- Centralization of Power: One of the central features of absolutism was the centralization of power in the hands of the monarch. The king or queen had control over all branches of government, including the military, the judiciary, and the administration. The monarchs eliminated rival centers of power, such as the nobility or regional governments, and established a system where all decisions flowed through the central authority.
- Divine Right of Kings: Monarchs ruled by the divine right of kings, meaning they believed their authority to govern came directly from God. This concept was used to justify the absolute power of the monarch, as it was believed that challenging the king’s authority was equivalent to challenging God’s will. The divine right theory often served to legitimize the monarch’s actions and make resistance to royal rule seem sinful.
- Lack of Checks on Power: Under absolutism, the monarch had little or no checks on their power. There were no democratic institutions, such as parliaments or representative bodies, that could limit or challenge royal authority. The king or queen exercised total control over the laws, the military, and foreign policy, and dissent or opposition was often suppressed.
- Strong Bureaucracy and Standing Armies: Monarchs built strong bureaucracies to help administer their realms. These bureaucrats were loyal to the king and worked to enforce royal policies. Standing armies, composed of professional soldiers rather than feudal levies, were maintained to protect the kingdom and enforce royal authority.
- Control Over Religion: Absolutist monarchs sought to control religion within their realms. In Catholic countries, this often meant asserting the monarch’s role as the protector of the faith and the ultimate authority on religious matters. In Protestant countries, kings and queens also asserted control over religious practices and sought to suppress religious dissent.
Absolutist Monarchs in Europe
Several European monarchs were prime examples of absolute rulers. Some of the most notable examples include:
- Louis XIV of France (1643–1715): Perhaps the most famous example of an absolutist monarch, Louis XIV, known as the “Sun King,” ruled France for over 70 years. He centralized power in the French monarchy, famously declaring, “L’État, c’est moi” (“I am the state”). Louis XIV strengthened the monarchy by reducing the power of the nobility and creating a system of royal control over the army, the economy, and the church. His lavish court at Versailles became the symbol of absolute power, and he used it to reinforce his authority over the nobility. Louis XIV’s reign, though marked by grandeur and cultural achievement, also faced significant financial strain due to costly wars.
- Peter the Great of Russia (1682–1725): Peter the Great was a transformative ruler who sought to modernize Russia and make it a major European power. He centralized political authority, built a strong army, and reformed Russian society along European lines. Peter the Great used his autocratic power to control the Russian Orthodox Church, modernize the economy, and expand Russia’s territory through military conquest, including the creation of the new capital city, St. Petersburg.
- Frederick the Great of Prussia (1740–1786): Frederick II, also known as Frederick the Great, was another example of an absolute ruler who consolidated power in Prussia. He expanded Prussian territory through military victories and was known for his enlightened absolutism, which aimed to combine absolute rule with reforms that improved the welfare of his subjects. Frederick the Great was a patron of the arts and philosophy but maintained strict control over the state.
- Charles I of England (1625–1649): While England experienced absolutism for a time under Charles I, his reign ended in the English Civil War and his execution. Charles I believed in the divine right of kings and sought to rule without Parliament, which led to tensions and conflict. His inability to maintain absolute control led to the English Revolution, and the establishment of constitutional monarchy following his death.
- Philip II of Spain (1556–1598): Philip II was a devout Catholic monarch who centralized power in Spain and sought to defend Catholicism across Europe. His reign saw the expansion of the Spanish Empire, the strengthening of royal authority, and the suppression of Protestantism. However, his policies also contributed to Spain’s eventual economic decline, as wars and the maintenance of the empire drained the treasury.
Decline of Absolutism
Despite the strength of absolute monarchies during the 17th and early 18th centuries, several factors contributed to the decline of absolutism in Europe:
- Economic Problems: Many absolutist monarchs spent vast amounts of money on wars, extravagant palaces, and lavish courts. The financial strain caused by constant warfare, coupled with inefficient taxation systems, weakened the economies of several monarchies. For example, Louis XIV’s wars and his extravagant spending led to severe debt and economic instability in France.
- Rise of Parliamentary Power: In countries like England, the rise of parliamentary power and the growing demand for representation by the people led to a gradual erosion of the absolute monarchy. The Glorious Revolution of 1688 in England, which resulted in the overthrow of King James II and the establishment of constitutional monarchy, is one of the key moments in the decline of absolutism.
- Enlightenment Ideas: The Enlightenment, an intellectual movement in the 18th century, promoted ideas of individual rights, liberty, and democracy. Philosophers like John Locke, Montesquieu, and Voltaire argued against absolute power and in favor of constitutional government, the separation of powers, and the protection of individual freedoms. These ideas influenced many European monarchs and contributed to the eventual decline of absolute monarchy.
- Revolutions: The French Revolution (1789) was the most significant event leading to the downfall of absolutism. The revolution marked the end of the Bourbon monarchy and the rise of republican ideals. The revolution also inspired other revolutionary movements across Europe, challenging the authority of absolute monarchs.
Conclusion
Absolutism in Europe was a period of centralized political power, where monarchs ruled with little or no checks on their authority. This system of governance, supported by the divine right of kings and a strong bureaucracy, allowed monarchs to exert control over all aspects of their states. However, the economic pressures of warfare, the rise of Enlightenment ideas, and the demand for democratic representation gradually led to the decline of absolutism. Although absolutism shaped much of Europe’s political landscape for centuries, the ideas of liberty, constitutionalism, and individual rights eventually gave rise to new forms of government, which would reshape the future of Europe.
2-(A) Growth of Absolute Monarchy in Spain and France.
स्पेन और फ्रांस में पूर्णराजतंत्र का उदय
यूरोप में आधुनिक काल में पूर्णराजतंत्र का उभार महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान, स्पेन और फ्रांस दोनों देशों में ऐसे शासक उभरे जिन्होंने अपनी सत्ता को एकत्रित किया, स्थानीय शाही परिवारों के प्रभाव को कम किया और केंद्रित और व्यक्तिगत शासन स्थापित किया। स्पेन के फिलिप द्वितीय और फ्रांस के लुई चौदहवें जैसे शासकों के शासनकाल ने पूर्णराजतंत्र के कुछ सबसे प्रतीकात्मक समय को दर्शाया। उनके कार्यों और नीतियों ने उनके देशों की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया और यूरोपीय इतिहास के प्रवाह को प्रभावित किया। यह निबंध स्पेन और फ्रांस में पूर्णराजतंत्र के उभार का अध्ययन करेगा, इसके कारणों, प्रमुख व्यक्तियों और इन राष्ट्रों और व्यापक यूरोप पर इसके प्रभाव को देखेगा।
स्पेन और पूर्णराजतंत्र का उदय
स्पेन की राजनीतिक संरचना का पृष्ठभूमि
स्पेन के पूर्णराजतंत्र की दिशा 15वीं और 16वीं शताब्दी के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों द्वारा आकारित हुई। मध्य युग के दौरान, स्पेन विभिन्न राज्यों जैसे कास्टाइल, अरागोन और नवरे में विभाजित था, जहां सत्ता का साझाकरण शाही परिवार और स्थानीय शाही परिवारों के बीच था। हालांकि, 15वीं शताबदी के अंत में कास्टाइल की इसाबेला I और अरागोन के फर्डिनेंड II की शादी के माध्यम से प्रमुख स्पेनी राज्य एकजुट हो गए, जिसने स्पेन के एक अधिक केंद्रीकृत राज्य के लिए आधार तैयार किया।
प्रारंभिक स्पेनिश राजतंत्र अभी भी अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर था, और शाही परिवार को शक्तिशाली शाही परिवार, कैथोलिक चर्च और मुस्लिम सेनाओं जैसे बाहरी खतरों के साथ संघर्ष करना पड़ा। 1492 में ग्रानाडा पर विजय प्राप्त करने के साथ रिकॉन्किस्टा का समापन हुआ, जो स्पेन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसने शाही परिवार को एकजुट किया और अपने क्षेत्रों पर शासन करने में मजबूत किया।
फिलिप द्वितीय और पूर्णराजतंत्र का उभार
स्पेन में पूर्णराजतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व फिलिप द्वितीय (1556-1598) था। उन्होंने अपने पिता चार्ल्स पंचम से एक विशाल साम्राज्य विरासत में प्राप्त किया, जिसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया में क्षेत्र शामिल थे। स्पेन साम्राज्य के आकार और जटिलता ने उन्हें अनूठी चुनौतियाँ प्रदान कीं, लेकिन फिलिप द्वितीय की केंद्रीकरण, धार्मिक आस्थाओं और सैन्य विस्तार की नीतियों ने उनकी सत्ता को मजबूती से स्थापित किया।
- शक्ति का केंद्रीकरण
फिलिप द्वितीय ने स्पेनिश राजतंत्र में सत्ता को केंद्रीत करने के लिए कई कदम उठाए। उनका एक प्रमुख कदम था कि वह शाही दरबार को मैड्रिड में स्थापित करें और स्पेन की राजनीतिक केंद्र के रूप में इसे स्थापित करें। उन्होंने स्थानीय शाही परिवारों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर सीधे नियंत्रण स्थापित किया और साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से नियंत्रित करने के लिए शाही अधिकारियों पर निर्भर रहे।
फिलिप ने कर्तेस (प्रतिनिधि विधानसभा) की भूमिका को भी सीमित किया और इसे केवल कर मामलों तक सीमित कर दिया, और क्षेत्रीय सरकारों को शाही आदेशों को चुनौती देने से रोका। यह शासन प्रणाली स्पेन में पूर्णराजतंत्र के सिद्धांतों को पहले पूरी तरह से लागू करने का एक महत्वपूर्ण कदम था।
- धार्मिक आस्थाएँ
फिलिप द्वितीय एक कट्टर कैथोलिक थे, और उनकी धार्मिक नीतियाँ स्पेन के राजतंत्र की प्रमुख विशेषता थीं। वह यूरोप में कैथोलिक धर्म की रक्षा करने वाले एक प्रमुख शासक के रूप में खुद को देख रहे थे, खासकर जब से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार यूरोप में फैलने लगा था। उनकी धार्मिक नीतियों का एक प्रसिद्ध उदाहरण स्पेनिश इनक्विजिशन का स्थापित होना था, जिसका उद्देश्य स्पेन और उसकी उपनिवेशों में प्रोटेस्टेंट धर्म और अन्य धार्मिक असहमति को दबाना था।
फिलिप की धार्मिक निष्ठा ने उनकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया, खासकर उनके इंग्लैंड के साथ संघर्ष में। 1588 में उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए स्पेनिश आर्माडा को भेजा, जो अंततः पराजित हुआ, लेकिन उनकी कैथोलिक निष्ठा उनके शासनकाल की एक स्थायी विशेषता रही।
- सैन्य विस्तार और आर्थिक दबाव
फिलिप द्वितीय के शासनकाल में, स्पेन ने यूरोप में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सैन्य उपायों का सहारा लिया। उनके शासनकाल में ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ कई युद्ध हुए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आठ वर्षों तक चला डच स्वतंत्रता संग्राम (1568-1648) था, जिसमें डच प्रदेशों ने स्पेन से स्वतंत्रता की मांग की थी। हालांकि, स्पेन की प्रारंभिक सैन्य सफलता रही, लेकिन युद्ध के लंबा खींचने से स्पेन की खजाने की स्थिति पर असर पड़ा और आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई।
फिर भी, स्पेन का साम्राज्य विश्व का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना रहा, खासकर इसके अमेरिका में विशाल उपनिवेशों के कारण। वहां से आने वाली चांदी और सोने की खदानों ने फिलिप के सैन्य अभियानों को वित्तीय सहायता प्रदान की, लेकिन इसी धन के कारण मुद्रास्फीति, आर्थिक कुप्रबंधन और बाहरी संसाधनों पर निर्भरता बढ़ी। ये आर्थिक समस्याएँ अंततः 17वीं शताबदी के अंत में स्पेन के पतन का कारण बनीं।
फिलिप द्वितीय के शासनकाल का प्रभाव
फिलिप द्वितीय का शासनकाल स्पेन और यूरोप पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। उनकी केंद्रीयकरण की नीतियाँ और धार्मिक आस्थाएँ स्पेन में पूर्णराजतंत्र को मजबूत करने में सहायक थीं, लेकिन सैन्य विस्तार और आर्थिक कुप्रबंधन ने स्पेन की शक्ति को कमजोर किया। उनके शासनकाल के अंत तक, स्पेन की यूरोप में प्रभुत्व की स्थिति कमजोर हो गई थी, हालांकि राजतंत्र एक शक्तिशाली संस्था के रूप में बना रहा।
फ्रांस और पूर्णराजतंत्र का उभार
फ्रांस की राजनीतिक संरचना का पृष्ठभूमि
फ्रांस में, पूर्णराजतंत्र का उभार 16वीं शताबदी के दौरान राजनीतिक केंद्रीकरण के परिणामस्वरूप हुआ, जिसे आंतरिक और बाहरी दबावों ने प्रभावित किया। फ्रांस का राजतंत्र लगातार शाही परिवारों के प्रभाव, धार्मिक संघर्षों और पड़ोसी शक्तियों के साथ क्षेत्रीय संघर्षों से जूझ रहा था। फ्रांस के धर्मयुद्ध (1562-1598) विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन युद्धों में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट (ह्यूगनोट्स) के बीच संघर्ष हुआ था, जिससे व्यापक हिंसा और अस्थिरता उत्पन्न हुई।
वाल्वॉय शाही परिवार, जो 14वीं शताबदी से फ्रांस पर शासन कर रहा था, युद्धों और शाही परिवारों की वफादारी में टूटने के कारण कमजोर पड़ गया। हालांकि, हेनरी चौथी (1589-1610) के शासनकाल ने राजतंत्र के केंद्रीकरण की नई दिशा की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने धार्मिक और नागरिक संघर्षों के बाद देश को एकजुट करने का प्रयास किया।
लुई XIII और कार्डिनल रिचलियू
फ्रांस में पूर्णराजतंत्र का वास्तविक उभार लुई XIII (1610–1643) और उनके प्रमुख मंत्री कार्डिनल रिचलियू के शासनकाल में हुआ। जबकि लुई XIII एक कमजोर और अप्रभावी शासक थे, रिचलियू ने फ्रांस की absolutist व्यवस्था का निर्माण किया।
- शक्ति का केंद्रीकरण
रिचलियू का उद्देश्य शाही परिवार की शक्ति को बढ़ाकर नobilों और अन्य प्रतिद्वंद्वी गुटों का प्रभाव समाप्त करना था। उन्होंने केंद्रीकरण की नीति अपनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरे फ्रांस में शाही सत्ता सर्वोच्च हो। रिचलियू ने स्थानीय प्रशासन की देखरेख करने के लिए शाही अधिकारियों के एक नेटवर्क का उपयोग किया, जिससे शाही परिवार की शक्ति को मज़बूती मिली और स्थानीय शाही परिवारों का प्रभाव घटा।
- नobilों का दमन
कार्डिनल रिचलियू ने फ्रांसीसी नobilों की राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने “इंटेंडेंट्स” की नीति शुरू की, जो क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्त करते थे और सीधे राजा से रिपोर्ट करते थे। ये अधिकारी अक्सर बोरजोआ (वाणिज्यिक वर्ग) से होते थे, जिससे शाही परिवार को शाही परिवारों को दरकिनार करने का अवसर मिलता था।
रिचलियू ने नobilों के महल नष्ट करने और उनकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की नीति अपनाई। इन नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि राजा की शक्ति पूर्णतया सर्वोच्च हो और नobilों का शाही सत्ता के लिए कोई चुनौती नहीं रहे।
- विदेश नीति और युद्ध
रिचलियू ने फ्रांस की विदेश नीति को भी आकार दिया, जो मुख्य रूप से स्पेन और हैब्सबर्ग साम्राज्य को कमजोर करने पर केंद्रित थी। उन्होंने तीस वर्ष के युद्ध (1618-1648) के दौरान प्रोटेस्टेंट शक्तियों के साथ गठबंधन किया, जैसे स्वीडन और डच गणराज्य। यह युद्ध फ्रांस की ताकत बढ़ाने और हैब्सबर्गों के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा था।
लुई XIV और पूर्णराजतंत्र का चरम
लुई XIV (1643-1715) के शासनकाल को फ्रांस में पूर्णराजतंत्र के चरम बिंदु के रूप में देखा जाता है। लुई XIV ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा शुरू की गई नीतियों को अपने शासन में विस्तार दिया और उन्हें पूरी तरह से लागू किया।
- शक्ति का केंद्रीकरण
लुई XIV ने प्रसिद्ध रूप से कहा, “L’État, c’est moi” (“मैं राज्य हूँ”), जो उनके केंद्रीयकरण की विचारधारा का प्रतीक था। उन्होंने शाही दरबार को वर्साय में स्थापित किया और वहां से राज्य मामलों का संचालन किया। दरबार में नobilों का दबाव और उनके प्रति वफादारी शाही परिवार की शक्ति को मज़बूती देती थी।
लुई XIV ने जनरल एस्स्टेट्स (प्रतिनिधि सभा) की भूमिका को समाप्त किया और बिना किसी विधायी निकाय से परामर्श किए शासन किया। राजा के निर्णय युद्ध, कराधान और शासन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों में शाही परिवार द्वारा किए गए थे।
- सैन्य और आर्थिक नियंत्रण
लुई XIV ने एक बड़ा और केंद्रीकृत सैन्य बनाए रखा, जिसे उन्होंने फ्रांस की रक्षा और विस्तार के लिए उपयोग किया। उनके युद्धों, जैसे स्पैनिश उत्तराधिकार युद्ध, ने फ्रांस के क्षेत्रीय अधिग्रहण को बढ़ाया, लेकिन उन्होंने फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला।
आर्थिक रूप से, लुई XIV ने राज्य के नियंत्रण में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों का पालन किया। उनके वित्त मंत्री, जीन-बैपटिस्ट कोलबर्ट के तहत, फ्रांस ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा, हालांकि युद्धों के विशाल खर्च ने खजाने को खाली किया और दीर्घकालिक वित्तीय समस्याओं को जन्म दिया।
लुई XIV के शासन का प्रभाव
लुई XIV का शासन फ्रांस और यूरोप पर एक स्थायी धरोहर छोड़ गया। उनका पूर्णराजतंत्र ने फ्रांस में राजनीतिक जीवन के केंद्र के रूप में शाही परिवार को मजबूती दी, लेकिन उनके युद्धों और विलासिता की वजह से राष्ट्रीय कर्ज बढ़ गया और फ्रांस में असंतोष भी पैदा हुआ। फिर भी, उनका शासन पूर्णराजतंत्र के चरम का प्रतीक बन गया और यूरोपीय राजनीतिक सोच और प्रथा पर गहरा प्रभाव छोड़ गया।
निष्कर्ष
स्पेन और फ्रांस में पूर्णराजतंत्र का उभार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकतों द्वारा प्रेरित था जिन्होंने इन देशों के मार्गदर्शन किया। स्पेन में फिलिप द्वितीय ने शक्ति का केंद्रीकरण किया और धार्मिक नीतियों के जरिए पूर्णराजतंत्र को मजबूत किया, जबकि फ्रांस में रिचलियू और लुई XIV ने इन विचारों को चरम सीमा तक पहुंचाया। शक्ति का केंद्रीकरण, नobilों का दमन और सैन्य और वित्तीय शक्ति का समेकन ने यूरोपीय राजनीति में पूर्णराजतंत्र की नींव रखी। हालांकि, युद्धों, आर्थिक कुप्रबंधन और प्रबुद्ध विचारों के बढ़ते प्रभाव ने पूर्णराजतंत्र के पतन की शुरुआत की, जिसने आधुनिक युग में नए शासन प्रणालियों को जन्म दिया।
2-(A) Growth of Absolute Monarchy in Spain and France.
The growth of absolute monarchy in Spain and France is one of the most significant political developments in early modern Europe. During the 16th and 17th centuries, both countries saw the emergence of monarchs who consolidated power in their own hands, reducing the influence of nobility and establishing highly centralized and personal rule. The reigns of monarchs such as Philip II of Spain and Louis XIV of France represent some of the most iconic periods of absolute monarchy. Their actions and policies helped define the political and social structures of their respective nations and influenced the course of European history. This essay will explore the rise of absolute monarchy in Spain and France, focusing on the causes, the key figures involved, and the impact on the nations and broader Europe.
Spain and the Rise of Absolute Monarchy
Background of Spain’s Political Structure
Spain’s rise to a centralized, absolute monarchy was shaped by the political, religious, and economic circumstances of the 15th and 16th centuries. During the Middle Ages, Spain was divided into several kingdoms, such as Castile, Aragon, and Navarre, with power shared between the monarchs and local nobility. However, in the late 15th century, the marriage of Isabella I of Castile and Ferdinand II of Aragon united the major Spanish kingdoms, forming the foundation for a more centralized Spanish state.
The early Spanish monarchy was still relatively weak compared to other European powers, and the monarchy had to contend with the powerful nobility, the influence of the Catholic Church, and various external threats, including Muslim forces. The Reconquista, the centuries-long campaign to expel Muslims from Spain, was completed in 1492 with the capture of Granada. This victory was significant in consolidating royal power as the monarchs, Isabella and Ferdinand, unified Spain and strengthened their control over the territories.
Philip II and the Rise of Absolute Power
The most important figure in the development of absolute monarchy in Spain was Philip II (reigned 1556–1598). He inherited a vast empire from his father, Charles V, which included territories in Europe, the Americas, and Asia. The size and complexity of the Spanish Empire presented unique challenges, but Philip II’s policies of centralization, religious orthodoxy, and military expansion helped solidify his authority.
- Centralization of Power
Philip II sought to centralize power in the Spanish monarchy, reducing the influence of local nobility. One of his primary strategies was to rule from a centralized location, the Royal Court in Madrid, which he established as the political center of Spain. He reduced the autonomy of local rulers by asserting direct control over Spain’s various regions, and he relied heavily on a bureaucratic system of royal officials to administer the empire.
Philip also reduced the power of the Spanish Cortes (the representative assembly) by limiting its role to matters of taxation and by curbing the ability of regional governments to challenge royal decrees. This shift in governance made Philip II one of the first monarchs to fully exercise the principles of absolute monarchy in Spain.
- Religious Orthodoxy
Philip II was a devout Catholic, and his religious policies were central to his vision of Spain’s monarchy. He saw himself as the defender of Catholicism in Europe, especially after the Protestant Reformation had begun to spread across Europe. One of the most notable examples of his religious policies was the establishment of the Spanish Inquisition, which sought to maintain Catholic orthodoxy and suppress Protestantism and other religious dissent within Spain and its territories.
Philip’s religious fervor also played a significant role in his foreign policy, particularly in his conflicts with Protestant countries. One of the most famous and disastrous decisions he made was the launching of the Spanish Armada in 1588 to invade England, a Protestant nation under the rule of Queen Elizabeth I. The defeat of the Armada marked the beginning of Spain’s decline as a dominant European power, but Philip’s commitment to Catholicism remained a defining feature of his reign.
- Military Expansion and Economic Strain
Under Philip II, Spain sought to expand its influence in Europe through military means. His reign was marked by several wars, including conflicts with the Ottoman Empire, France, and England. The most significant of these was the Eighty Years’ War (1568–1648) against the Dutch provinces, which sought independence from Spanish rule. Although Spain initially had some military successes, the prolonged nature of the conflict drained the Spanish treasury and led to economic instability.
Despite these military setbacks, Spain’s empire remained one of the most powerful in the world, particularly due to its vast colonial holdings in the Americas. The influx of silver and gold from Spanish colonies helped fund Philip’s military campaigns, but the wealth also led to inflation, economic mismanagement, and a dependence on external resources. These economic difficulties eventually contributed to the decline of Spain’s power in the 17th century.
Impact of Philip II’s Reign
Philip II’s reign had a profound impact on Spain and its place in Europe. His efforts to centralize power and impose religious orthodoxy helped solidify the absolute monarchy, but his military overreach and economic mismanagement weakened the Spanish state. By the end of his reign, Spain’s dominance in Europe had begun to wane, though the monarchy remained a powerful institution for many years.
France and the Rise of Absolute Monarchy
Background of France’s Political Structure
In France, the rise of absolute monarchy can be traced back to the centralization of power during the 16th century, a process that was influenced by both internal and external pressures. The French monarchy had been struggling with the influence of the nobility, religious conflicts, and territorial disputes with neighboring powers. The French Wars of Religion (1562–1598) were particularly significant, as they pitted Catholics against Protestants (Huguenots) and resulted in widespread violence and instability.
The Valois monarchy, which had ruled France since the 14th century, was weakened by the wars and the fracturing of the nobility’s loyalty. However, the reign of Henry IV (1589–1610) marked the beginning of a new phase in the consolidation of royal power, as he sought to unify the country after years of religious and civil conflict.
Louis XIII and Cardinal Richelieu
The true rise of absolute monarchy in France, however, occurred during the reign of Louis XIII (1610–1643) and his chief minister, Cardinal Richelieu. While Louis XIII was a weak and ineffective monarch, Richelieu was the architect of France’s absolutist system.
- Centralization of Power
Richelieu’s goal was to strengthen the monarchy by diminishing the power of the nobility and other rival factions, such as the Huguenots and the regional parlements (courts). He pursued a policy of centralization, ensuring that royal authority was supreme throughout France. Richelieu used a network of royal officials to oversee local administration, reducing the power of local lords who had traditionally held significant authority over their regions.
Richelieu also curtailed the independence of the Huguenots, who had their own fortified cities and armies. In 1628, he besieged the Huguenot stronghold of La Rochelle, forcing the Huguenots to accept royal authority. This marked a significant step in the consolidation of royal power, as it reduced the influence of religious and regional factions.
- Suppression of Nobility
Cardinal Richelieu worked to undermine the political power of the French nobility. He introduced a policy of “intendants,” royal officials who were appointed to oversee provinces and report directly to the king. These officials were often chosen from the bourgeoisie rather than the nobility, which allowed the monarchy to bypass the traditional nobility in the administration of the kingdom.
Richelieu also engaged in a campaign to break the power of the nobility through the destruction of their castles and the weakening of their military capabilities. His policies helped ensure that the king’s authority was absolute and that the nobility no longer posed a significant challenge to royal power.
- Foreign Policy and Wars
Richelieu was also a key figure in shaping France’s foreign policy, which was aimed at weakening Spain and the Habsburgs, France’s main rivals in Europe. He pursued a policy of alliance with Protestant powers, such as Sweden and the Dutch Republic, during the Thirty Years’ War (1618–1648). This involvement in the war was part of Richelieu’s broader strategy to weaken the power of the Habsburgs and increase French influence in Europe.
Louis XIV and the Apex of Absolute Monarchy
The reign of Louis XIV (1643–1715), often referred to as the “Sun King,” is widely regarded as the epitome of absolute monarchy in France. Louis XIV inherited the work of his predecessors and took it to its fullest expression.
- Centralization of Power
Louis XIV famously stated, “L’État, c’est moi” (“I am the state”), which encapsulated his belief in the centralization of power in the monarchy. Louis XIV furthered the process of centralization by creating an elaborate system of government centered around the royal court at Versailles. The king’s personal control over state affairs was reinforced by his domination of the court, where the nobility was required to attend and remain loyal to him in order to secure privileges.
Louis XIV effectively abolished the role of the estates general (the representative assembly) and ruled without the need for consultation with any legislative body. The king’s decisions on war, taxation, and governance were made solely by him and his close circle of ministers.
- Military and Economic Control
Louis XIV maintained a large and highly centralized military, which he used to defend France and expand its territory. His wars, such as the War of Spanish Succession, significantly increased France’s territorial holdings but also placed a great strain on the French economy.
Economically, Louis XIV pursued policies that promoted mercantilism, aiming to increase France’s wealth through state control of industry and trade. Under his finance minister, Jean-Baptiste Colbert, France saw significant economic growth, although the immense costs of warfare drained the treasury and created long-term financial problems.
Impact of Louis XIV’s Reign
Louis XIV’s reign left a lasting legacy on France and Europe. His absolute rule solidified the French monarchy as the center of political life in France, but it also created challenges. His wars and lavish spending led to a mounting national debt, and his oppressive policies toward the nobility alienated some segments of French society. Nevertheless, his reign marked the height of absolute monarchy and left a lasting impact on European political thought and practice.
Conclusion
The rise of absolute monarchy in Spain and France was driven by political, economic, and social forces that shaped the trajectory of both countries during the early modern period. In Spain, Philip II’s centralization of power and religious policies contributed to the growth of absolute monarchy, while in France, figures like Cardinal Richelieu and Louis XIV took these ideas to their zenith. The policies of centralization, the suppression of the nobility, and the consolidation of military and financial power helped establish absolute monarchies that would dominate European politics for centuries. However, the challenges of warfare, economic mismanagement, and the growing influence of Enlightenment ideas eventually led to the decline of absolute monarchy, paving the way for new political systems in the modern era.
2-(B) Absolute Monarchy in Britain and the Struggle with Parliament.
ब्रिटेन में पूर्ण राजशाही और संसद के साथ संघर्ष
ब्रिटेन में पूर्ण राजशाही का विकास और इसके बाद संसद के साथ संघर्ष, इंग्लैंड के राजनीतिक विकास के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। फ्रांस और स्पेन जैसे अन्य यूरोपीय देशों में जहां पूर्ण राजशाही को राजाओं जैसे लुई XIV (फ्रांस) और फिलिप II (स्पेन) के तहत अपने चरम पर पहुँचने का अवसर मिला, वहीं इंग्लैंड का अनुभव एक निरंतर संघर्ष था, जिसमें राजशाही और संसद के बीच एक तनावपूर्ण रिश्ते को देखा गया। ब्रिटिश राजशाही ने सत्ता के केन्द्रीकरण और समेकन की कोशिश की, लेकिन यह लगातार राजनीतिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक संरचनाओं से चुनौती प्राप्त करती रही। इस संघर्ष ने इंग्लिश गृहयुद्ध (English Civil War), किंग चार्ल्स I की हत्या, और ओलिवर क्रॉमवेल के तहत इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ (गणराज्य) की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया।
राजशाही और संसद के बीच यह संघर्ष न केवल राजनीतिक विचारधाराओं का युद्ध था, बल्कि यह आर्थिक और धार्मिक कारणों से भी प्रेरित था, जिसने इंग्लैंड के इतिहास की दिशा को आकार दिया। यह निबंध ब्रिटेन में पूर्ण राजशाही के उदय, राजशाही और संसद के बीच संघर्ष के कारणों, प्रमुख घटनाओं और इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों की व्याख्या करेगा।
ब्रिटेन में पूर्ण राजशाही का उदय
टुडर वंश और केंद्रीकरण की शुरुआत
ब्रिटेन में पूर्ण राजशाही की जड़ें टुडर वंश से जुड़ी हैं, जिसकी सत्ता 1485 में हेनरी VII के तहत शुरू हुई थी। टुडर राजवंश ने विभिन्न यंत्रणाओं के माध्यम से राजकीय शक्ति को समेकित किया। हेनरी VII के शासनकाल में, युद्धों के बाद राजशाही को पुनः सशक्त किया गया, जिसने वॉर्स ऑफ द रोजेस (Wars of the Roses) के बाद राजसत्ता को मजबूत किया। हेनरी VIII ने इस प्रक्रिया को और बढ़ाया, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च से अलग होकर इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करके। यह धार्मिक और राजनीतिक कदम था, क्योंकि इसने हेनरी को धार्मिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर दिया और कैथोलिक चर्च और पोप की शक्ति को सीमित किया।
हेनरी के उत्तराधिकारी, विशेष रूप से एलिजाबेथ I, ने राजशाही की शक्ति को सुदृढ़ किया, हालांकि उन्होंने संसद की शक्ति को भी सम्मान दिया और अपने शासन को सुलह और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित रखा। एलिजाबेथ I के शासनकाल में राजशाही मजबूत हुई, लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि संसद के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है, ताकि साम्राज्य की स्थिरता बनी रहे। हालांकि उनका शासन अन्य यूरोपीय सम्राटों के पूर्ण राजशाही के स्तर तक नहीं पहुँचा, लेकिन उन्होंने राजशाही के अधिकारों का अतिक्रमण करने की बजाय संसद के साथ काम करने का प्रयास किया।
स्टुअर्ट वंश और पूर्ण राजशाही की ओर झुकाव
ब्रिटेन में पूर्ण राजशाही के संघर्ष की शुरुआत 1603 में जेम्स I के शासन से होती है। जेम्स I स्कॉटलैंड में शासन करते हुए इंग्लैंड के सिंहासन पर चढ़े थे। उन्होंने भगवान के अधिकार से शासक होने का सिद्धांत अपनाया, जिसे वह स्कॉटलैंड में अनुभव कर चुके थे। जेम्स I का मानना था कि सम्राट केवल भगवान के प्रति जिम्मेदार होता है और संसद को राजशाही के अधिकारों के सामने खुद को झुका देना चाहिए।
जेम्स I के बाद, उनके पुत्र चार्ल्स I ने भी अपने पिता के विचारों को अपनाया, लेकिन इसे और अधिक बढ़ा दिया। चार्ल्स I का मानना था कि वह भगवान द्वारा नियुक्त किए गए शासक हैं और उन्हें बिना संसद की सहमति के शासन करने का अधिकार है। उनके इस विचार ने संसद के साथ टकराव को बढ़ावा दिया।
राजशाही और संसद के बीच संघर्ष
चार्ल्स I और शॉर्ट और लॉन्ग पार्लियामेंट्स
चार्ल्स I के शासन में, उन्होंने बिना संसद के शासन करने का प्रयास किया। 1628 में, उन्हें संसदीय विरोध के कारण संसद को फिर से बुलाना पड़ा। इस समय पर पिटीशन ऑफ राइट नामक एक दस्तावेज़ पारित किया गया, जो सम्राट की शक्ति को सीमित करता था और संसद की अनुमति के बिना कर लगाने को अवैध ठहराता था। हालांकि, चार्ल्स ने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में उनकी नीतियाँ वही रही, जिनसे संसद के अधिकारों की अनदेखी की गई।
चार्ल्स I ने 1629 में संसद को फिर से भंग कर दिया और अगले ग्यारह वर्षों तक बिना संसद के शासन किया, जिसे “पर्सनल रूल” (Personal Rule) कहा जाता है। हालांकि, चार्ल्स के शासन में कई संकट उत्पन्न हुए, जिनमें स्कॉटलैंड के साथ युद्ध भी शामिल था। इस आर्थिक दबाव और सैन्य असफलताओं के कारण उन्हें 1640 में संसद को फिर से बुलाना पड़ा, जो “लॉन्ग पार्लियामेंट” के नाम से जाना जाता है।
लॉन्ग पार्लियामेंट और बढ़ता संघर्ष
लॉन्ग पार्लियामेंट में ऐसे कई सदस्य थे, जो चार्ल्स I की तानाशाही और संसद की शक्ति को नजरअंदाज करने के खिलाफ थे। पार्लियामेंट ने चार्ल्स के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया और कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया, जैसे कि ट्रायनीअल एक्ट (Triennial Act), जिसने यह सुनिश्चित किया कि संसद हर तीन साल में एक बार जरूर बुलाई जाएगी। इसके अलावा, 1640 में, आर्चबिशप लॉड को अपदस्थ किया गया, जो चार्ल्स के करीबी सहयोगी थे।
चरण दर चरण, संसद और चार्ल्स I के बीच टकराव बढ़ता गया। चार्ल्स ने पांच सदस्य पार्लियामेंट के नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसे संसद के प्रति आक्रमण के रूप में देखा गया। इससे इंग्लिश गृहयुद्ध का आगाज हुआ।
इंग्लिश गृहयुद्ध
इंग्लिश गृहयुद्ध (1642-1651) सीधे तौर पर राजशाही और संसद के बीच संघर्ष के कारण हुआ। युद्ध का मुख्य संघर्ष किंग चार्ल्स I (रॉयलिस्ट्स/कावालियर) और संसद (राउंडहेड्स) के बीच था। राउंडहेड्स के नेता ओलिवर क्रॉमवेल ने एक सुसंगत सेना बनाई, जिसे न्यू मॉडल आर्मी कहा गया। युद्ध के दौरान धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉयलिस्ट्स आम तौर पर ऐंग्लिकन थे, जबकि राउंडहेड्स में प्यूरीटन्स और अन्य धार्मिक समूह शामिल थे जो राजशाही की धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट थे।
1646 में चार्ल्स I को हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि, संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। संसद के भीतर भी राजनीतिक विभाजन था, और चार्ल्स I का भाग्य अनिश्चित था। अंततः, 1649 में चार्ल्स I को राजद्रोह के आरोप में मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई, और यह इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार था जब किसी सम्राट को उनके ही लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया गया।
कॉमनवेल्थ और इंटररेग्नम
चार्ल्स I की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई, जिसके नेता ओलिवर क्रॉमवेल थे। क्रॉमवेल का शासन सैन्य अधिनायकवाद पर आधारित था, और यह एक रिपब्लिक था, हालांकि इसमें राजशाही की जगह एक केंद्रीकृत शक्ति स्थापित की गई थी। क्रॉमवेल स्वयं लार्ड प्रोटेक्टर बन गए, और उनके शासनकाल में कई सुधार किए गए। हालांकि, उनके शासन में प्यूरीटन नैतिक कोड के लागू होने और स्थिरता की कमी के कारण कॉमनवेल्थ का दौर अप्रिय था। 1660 में क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद, राजशाही फिर से बहाल हुई और चार्ल्स II के शासनकाल की शुरुआत हुई।
ग्लोरियस रिवोल्यूशन और पूर्ण राजशाही का अंत
ब्रिटेन में पूर्ण राजशाही को अंतिम रूप से खत्म करने वाली घटना 1688 में हुई, जिसे “ग्लोरियस रिवोल्यूशन” कहा जाता है। चार्ल्स II के बाद, उनके भाई जेम्स II का शासन आया, जिनके कैथोलिक रुझान और निरंकुश शासन के कारण व्यापक असंतोष फैल गया। संसद ने डर के कारण विलियम ऑफ ऑरेन्ज़ को इंग्लैंड पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। जेम्स II देश छोड़कर भाग गए और विलियम और उनकी पत्नी मैरी को संयुक्त रूप से सम्राट घोषित किया गया।
ग्लोरियस रिवोल्यूशन के परिणामस्वरूप 1689 में बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) पारित हुआ, जिसने राजशाही की शक्ति को सीमित किया और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इस दस्तावेज़ ने यह सुनिश्चित किया कि सम्राट संसद की अनुमति के बिना कर नहीं लगा सकता, संसद के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और शांति काल में बिना संसद की स्वीकृति के स्थायी सेना नहीं रख सकता।
निष्कर्ष
ब्रिटेन में पूर्ण राजशाही का उदय और गिरावट, राजशाही और संसद के बीच संघर्ष का एक निरंतर इतिहास है। जबकि जेम्स I और चार्ल्स I जैसे सम्राटों ने पूर्ण राजशाही की स्थापना की कोशिश की, लेकिन वे संसद के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से लगातार चुनौती पाते रहे। 17वीं सदी के संघर्षों ने, विशेष रूप से इंग्लिश गृहयुद्ध और ग्लोरियस रिवोल्यूशन ने ब्रिटेन में संवैधानिकता को जन्म दिया। ग्लोरियस रिवोल्यूशन के बाद, ब्रिटेन में राजशाही ने एक औपचारिक और प्रतीकात्मक भूमिका निभाई, जबकि वास्तविक शक्ति संसद के पास चली गई। यह संघर्ष ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के आधुनिक रूप को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें संसद को सर्वोच्चता प्राप्त हुई और पूर्ण राजशाही को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया।
2-(B) Absolute Monarchy in Britain and the Struggle with Parliament.
The development of absolute monarchy in Britain and the eventual struggle with Parliament represents one of the most pivotal chapters in the history of English political evolution. Unlike other European countries such as France and Spain, where absolute monarchy reached its zenith under kings like Louis XIV of France and Philip II of Spain, England’s experience was marked by a constant tug-of-war between the monarchy and Parliament. The English monarchy’s attempt to centralize and consolidate power eventually led to the breakdown of royal authority, culminating in the English Civil War, the execution of King Charles I, and the establishment of the Commonwealth under Oliver Cromwell.
The relationship between monarchy and Parliament in Britain was complicated by a number of cultural, historical, and political factors. The English monarchy attempted to assert absolute power, but was constantly checked by the evolving constitutional and political structures that formed the basis for parliamentary rule. This struggle was not only a battle of political ideology but also of economic and religious factors that helped shape the course of English history. This essay will explore the rise of absolute monarchy in Britain, the causes of the struggle between the monarchy and Parliament, the key events, and how the conflict eventually resulted in significant changes in the structure of English governance.
The Rise of Absolute Monarchy in Britain
The Tudor Dynasty and the Beginnings of Centralization
The roots of absolute monarchy in Britain can be traced back to the Tudor dynasty, which came to power in 1485 with Henry VII. The Tudors were able to consolidate royal power through a variety of mechanisms. Henry VII’s reign marked the beginning of centralization in England after the Wars of the Roses, which had left the monarchy weak and divided. Henry VIII further strengthened royal authority, notably through his break with the Roman Catholic Church and the establishment of the Church of England. This move was not only religious but also political, as it allowed Henry to centralize control over religious matters, diminishing the influence of the Catholic Church and the Pope.
Henry’s successors, particularly Elizabeth I, solidified the power of the monarchy, though Elizabeth maintained a delicate balance between royal authority and the power of Parliament. Elizabeth’s reign (1558–1603) saw the development of a strong monarchy, but she recognized the importance of working with Parliament for the stability of the kingdom. While her reign did not feature the level of absolutism seen in other European monarchs, she did assert royal prerogatives over matters like taxation and foreign policy.
The Stuart Dynasty and the Drive for Absolute Power
The struggle between monarchy and Parliament intensified after the accession of the Stuart monarchs, beginning with James I in 1603. James was the first monarch to attempt the establishment of absolute monarchy in Britain. He inherited the English throne after the death of Elizabeth I and brought with him the ideals of divine right of kings, which he had learned during his rule in Scotland. James I believed that the monarch was answerable only to God and that Parliament’s power should be subordinated to royal authority.
James I’s belief in the divine right of kings led to several confrontations with Parliament. He attempted to bypass Parliament on matters of taxation and governance, often acting unilaterally in foreign policy. James’s son, Charles I, continued his father’s policies but took them to extremes. Charles’s belief in his divine right to rule led him to dissolve Parliament on several occasions when it refused to grant him the taxes he desired, particularly in the early 1620s. This disregard for parliamentary power set the stage for the eventual conflict between the monarchy and Parliament that would lead to the English Civil War.
The Struggle Between the Monarchy and Parliament
Charles I and the Short and Long Parliaments
Charles I’s attempts to rule without Parliament and his growing need for funds to support his military campaigns led to increased tensions. One of the most significant events in this period was Charles’s attempt to impose ship money, a tax traditionally levied in coastal regions during times of war, on the entire country, even during peacetime. This action was highly unpopular and led to widespread resistance. The king’s determination to raise funds without Parliament’s approval alienated many members of the English elite, who saw this as an abuse of royal prerogative.
In 1628, Charles I was forced to recall Parliament due to a shortage of funds, leading to the Petition of Right, a document that limited the king’s ability to impose taxes without parliamentary consent and prohibited arbitrary imprisonment. Charles reluctantly agreed to sign the Petition of Right, but his subsequent actions showed his continuing disregard for parliamentary power. In 1629, Charles dissolved Parliament for the last time and began governing without it for the next eleven years, a period often referred to as the Personal Rule.
However, Charles’s Personal Rule faced significant challenges. By 1637, the king attempted to impose a new prayer book on Scotland, which led to the Bishops’ Wars. The cost of these wars and the need for funds to support his military campaign forced Charles to call Parliament once again in 1640. This was the beginning of the Short Parliament, which lasted only three weeks before Charles dissolved it. However, the financial strain and military failure led Charles to call another Parliament in November 1640, known as the Long Parliament.
The Long Parliament and the Growing Conflict
The Long Parliament, which sat from 1640 to 1660, was one of the most significant events in the struggle between the monarchy and Parliament. Members of Parliament, many of whom had grown frustrated with Charles’s authoritarian rule, sought to limit the king’s powers and increase their own influence. One of the first acts of the Long Parliament was the impeachment of Archbishop Laud, who had been a close adviser to the king and a symbol of his policies. Parliament also passed the Triennial Act, which required that Parliament be called at least once every three years, effectively removing the king’s ability to dissolve Parliament at will.
In addition to these political reforms, tensions between Charles and Parliament escalated over the question of control of the army. The king’s efforts to arrest five members of Parliament in 1642—an attempt to suppress dissent—was seen as a direct attack on parliamentary privilege. This act of aggression led to the outbreak of the English Civil War.
The English Civil War
The English Civil War (1642–1651) was the direct result of the escalating conflict between the monarchy and Parliament. The war was fought between the forces of King Charles I, known as the Royalists or Cavaliers, and those of Parliament, known as the Roundheads. The Roundheads were led by figures such as Oliver Cromwell, who was able to organize and lead a disciplined parliamentary army, the New Model Army.
The conflict was not simply a power struggle between the monarchy and Parliament but was also driven by underlying religious and social factors. The Royalists were largely composed of the Anglican aristocracy, while the Roundheads included Puritans, Presbyterians, and other religious groups that were disillusioned with the monarchy’s religious policies. The war saw the rise of radical political and religious ideas, including the Levellers, who advocated for greater democracy and equality.
In 1646, after a series of defeats, Charles I was forced to surrender. However, the conflict did not end there. The political divisions within Parliament led to further tensions, and the king’s fate remained uncertain. In 1649, Charles I was tried and executed for treason, marking the first time in English history that a monarch was publicly put to death by his subjects.
The Commonwealth and the Interregnum
Following the execution of Charles I, England was declared a Commonwealth under the leadership of Oliver Cromwell. Cromwell’s government was a military dictatorship, and though it was ostensibly a republic, it effectively replaced the monarchy with a centralized form of power. The period of the Commonwealth, known as the Interregnum (1649–1660), was marked by attempts to create a republican system of government. Cromwell himself became Lord Protector, exercising powers that were more monarchical than republican.
Despite some reforms, the Commonwealth period was unpopular, particularly due to the imposition of Puritan moral codes and the lack of stability. In 1660, after Cromwell’s death, the monarchy was restored with the accession of Charles II, the son of the executed Charles I. The Restoration of the monarchy, however, did not mark the end of tensions between monarchy and Parliament.
The Glorious Revolution and the End of Absolute Monarchy
The final blow to the concept of absolute monarchy in Britain came with the Glorious Revolution of 1688. Charles II had been succeeded by his brother James II, whose openly Catholic sympathies and autocratic rule led to widespread discontent. Parliament, fearful of the potential for a Catholic dynasty, invited William of Orange, the Dutch Protestant prince, to invade England. James II fled the country, and William and his wife, Mary, were declared joint monarchs.
The Glorious Revolution resulted in the Bill of Rights (1689), which curtailed the power of the monarchy and set forth the supremacy of Parliament. This document established that the king could not levy taxes without Parliament’s consent, could not interfere in parliamentary elections, and could not maintain a standing army in peacetime without parliamentary approval. The Glorious Revolution effectively ended the idea of absolute monarchy in Britain and laid the foundation for a constitutional monarchy.
Conclusion
The rise and fall of absolute monarchy in Britain was marked by a continuous struggle between the monarchy and Parliament. While monarchs like James I and Charles I attempted to assert absolute power, they were consistently challenged by Parliament’s growing political power. The conflicts of the 17th century, including the English Civil War and the Glorious Revolution, were pivotal in the development of British constitutionalism. By the end of the Glorious Revolution, the monarchy in Britain had been irrevocably altered, with parliamentary supremacy established and absolute monarchy permanently discarded. This struggle set the stage for the modern British political system, where the monarchy serves a ceremonial role and Parliament holds the true power.
2-(C) Absolutism in Austria and Russia, Conflict in Germany.
ऑस्ट्रिया और रूस में पूर्ण राजशाही, और जर्मनी में संघर्ष
यूरोप में प्रारंभिक आधुनिक काल में पूर्ण राजशाही का उदय यूरोपीय राज्यों में शक्ति के संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। पूर्ण राजशाही, जिसमें शासक राज्य और इसके लोगों पर सर्वोच्च अधिकार रखते थे, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के कई देशों के राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ऑस्ट्रिया और रूस, जो पूर्वी यूरोप की महान शक्तियाँ थीं, वे दो ऐसे देश थे जहां पूर्ण राजशाही का विकास हुआ, जबकि जर्मन-भाषी भूमि अपने विशिष्ट राजनीतिक संरचनाओं के कारण संघर्ष का सामना कर रही थी, विशेष रूप से पवित्र रोमन साम्राज्य की जटिलता के कारण। इस निबंध में हम ऑस्ट्रिया और रूस में पूर्ण राजशाही के विकास, उनके सामने आने वाली चुनौतियों, और जर्मन-भाषी भूमि में संघर्षों का विश्लेषण करेंगे, विशेष रूप से तीस वर्षीय युद्ध पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
ऑस्ट्रिया में पूर्ण राजशाही
हैब्सबर्ग वंश का उदय
ऑस्ट्रिया में पूर्ण राजशाही का इतिहास हैब्सबर्ग वंश से जुड़ा हुआ है, जो कई शताब्दियों तक ऑस्ट्रिया और मध्य यूरोप पर राज करता था। हैब्सबर्गों का उदय 15वीं शताब्दी में हुआ, जब उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राजवंशीय विवाहों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। 16वीं शताब्दी तक, हैब्सबर्ग यूरोप के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक बन गए थे, और उन्होंने ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, हंगरी, और इटली तथा नीदरलैंड्स के कुछ हिस्सों पर शासन किया।
सम्राट चार्ल्स V (1519–1556) के शासनकाल में, हैब्सबर्ग साम्राज्य यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राज्य था। लेकिन उनकी त्यागपत्र के बाद, साम्राज्य को उनके पुत्र, स्पेन के फिलिप II और उनके भाई, फर्डिनेंड I में बाँट दिया गया, जो पवित्र रोमन सम्राट बने और ऑस्ट्रियाई भूमि पर शासन किया। फर्डिनेंड के वंशजों के शासनकाल में ऑस्ट्रिया पूर्ण राजशाही की ओर बढ़ा।
हैब्सबर्गों के तहत पूर्ण राजशाही की स्थापना
17वीं शताब्दी में, विशेष रूप से सम्राट लियोपोल्ड I (1658–1705) के शासनकाल में, हैब्सबर्गों ने अपनी शक्ति को केंद्रीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। लियोपोल्ड I एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने ऑस्ट्रिया के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से हंगरी और बोहेमिया में विद्रोहों से निपटने के लिए संघर्ष किया। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, लियोपोल्ड ने सामंती शक्ति को कम करने और अपने अधिकार को विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास किया।
ऑस्ट्रिया के पूर्ण राजशाही के लिए एक महत्वपूर्ण घटना उस समय की थी जब लियोपोल्ड I ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त की, विशेष रूप से 1683 में वियना की लड़ाई में, जहां हैब्सबर्गों ने यूरोपीय सहयोगियों की मदद से ऑटोमन साम्राज्य को हराया और मध्य यूरोप पर उनके प्रभाव को समाप्त किया।
मारिया टेरेसा और पूर्ण राजशाही की अंतिम स्थापना
मारिया टेरेसा (1740–1780) के शासनकाल में ऑस्ट्रिया की पूर्ण राजशाही का शिखर देखा गया। मारिया टेरेसा ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए। उन्होंने सामंती शक्ति को कम करने और अपने शासन को केंद्रीकृत करने के लिए कई कदम उठाए। इन सुधारों में सैन्य और आर्थिक नीतियाँ शामिल थीं, जिनका उद्देश्य सम्राट की शक्ति को मजबूत करना और साम्राज्य को स्थिर करना था।
उनके पुत्र जोसेफ II (1780–1790) ने और भी दूरदर्शी सुधारों की योजना बनाई, जिसमें चर्च की शक्ति को सीमित करना और सम्राट की शक्ति को और भी अधिक केंद्रीकृत करना शामिल था। हालांकि, जोसेफ के सुधारों ने कुछ क्षेत्रों में विद्रोह को जन्म दिया, और उनके बाद उनके अधिकांश सुधारों को उलट दिया गया। फिर भी, मारिया टेरेसा और जोसेफ II ने ऑस्ट्रिया में पूर्ण राजशाही की नींव रखी, जिससे हब्सबर्ग साम्राज्य के अधिकार को मजबूत किया गया।
रूस में पूर्ण राजशाही
रोमानोव वंश का उदय
रूस में पूर्ण राजशाही का इतिहास मुख्य रूप से रोमानोव वंश से जुड़ा हुआ है, जिसने 1613 से 1917 तक रूस पर शासन किया। रोमानोवों ने रूस में समय संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बाद अपनी शक्ति स्थापित की। वे रूस के साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने साथ ही राज्य में पूर्ण राजशाही की स्थापना की।
पीटर द ग्रेट और रूस का परिवर्तन
रूस में पूर्ण राजशाही का सबसे महत्वपूर्ण विकास पीटर द ग्रेट (1682–1725) के शासनकाल में हुआ। पीटर ने रूस को एक आधुनिक यूरोपीय शक्ति बनाने का सपना देखा और उनके शासन में कई क्रांतिकारी सुधार किए गए। उन्होंने रूस की सेना और नौसेना को आधुनिक बनाया, ताकि रूस यूरोप में एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बन सके। इसके अलावा, पीटर ने सामंती शक्ति को कम करने और सम्राट की शक्ति को केंद्रीकृत करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए।
पीटर द ग्रेट का एक प्रमुख योगदान था सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना, जिसे उन्होंने रूस के पश्चिमीकरण और यूरोप के साथ रूस के संबंधों को मजबूत करने के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उनके शासन में रूस ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य के रूप में अपनी स्थिति बनाई, जिसने रूस में पूर्ण राजशाही की स्थापना की नींव रखी।
कैथरीन द ग्रेट और रूस का विस्तार
कैथरीन द ग्रेट (1762–1796) ने पीटर द ग्रेट द्वारा शुरू किए गए सुधारों को आगे बढ़ाया और रूस को और भी अधिक केंद्रीयकृत किया। उन्होंने रूस के साम्राज्य को विस्तारित किया, विशेष रूप से पोलैंड के विभाजन के माध्यम से, और रूस को एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि, उन्होंने अपने शासन के दौरान कई सुधार किए, लेकिन वे एक पूर्ण राजशाही की नीति पर भी विश्वास करती थीं, जिसमें सम्राट का सर्वोच्च अधिकार था।
कैथरीन का शासन, जो रूस के सामंती वर्ग की समृद्धि के लिए जाना जाता था, ने रूस की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को मजबूत किया, हालांकि उनके शासन में भी सेवकों और किसानों के साथ सामाजिक असंतोष था, विशेष रूप से सर्वेन्ट सिस्टम के कारण।
जर्मनी में संघर्ष: तीस वर्षीय युद्ध
पवित्र रोमन साम्राज्य और धार्मिक तनाव
जर्मन-भाषी भूमि में संघर्ष का मुख्य कारण पवित्र रोमन साम्राज्य की राजनीतिक संरचना थी, जिसमें कई स्वतंत्र राज्य और क्षेत्र शामिल थे, जो सम्राट के अधिकारों से स्वतंत्र रूप से शासित थे। पवित्र रोमन सम्राट की शक्ति सीमित थी, और साम्राज्य के भीतर राज्य और प्रिंस अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते थे।
तीस वर्षीय युद्ध (1618–1648) यूरोप के इतिहास का एक सबसे विनाशकारी युद्ध था, जो मुख्य रूप से धार्मिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, जब पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया था। युद्ध ने धार्मिक संघर्ष को बढ़ाया और युद्ध में कई यूरोपीय शक्तियाँ शामिल हो गईं, जिनमें स्वीडन, फ्रांस और स्पेन शामिल थे।
तीस वर्षीय युद्ध का विनाश
तीस वर्षीय युद्ध ने जर्मन भूमि में व्यापक तबाही मचाई। यह युद्ध न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि राजनीतिक कारणों से भी लड़ा गया था, और इसने जर्मनी के कई हिस्सों में युद्ध, अकाल, और महामारी फैलायी। युद्ध ने पवित्र रोमन साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया और 1648 में वेस्टफालिया की शांति संधि द्वारा इस संघर्ष का अंत हुआ।
वेस्तफालिया संधि ने पवित्र रोमन साम्राज्य के भीतर कई जर्मन राज्यों को स्वतंत्रता दी और साम्राज्य की शक्ति को और अधिक सीमित किया। इसने धार्मिक विभाजन को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और जर्मनी को एक और अधिक विभाजित राजनीतिक परिदृश्य में छोड़ दिया, जो भविष्य में जर्मन एकता को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख बाधा बना।
निष्कर्ष
ऑस्ट्रिया और रूस में पूर्ण राजशाही का विकास और जर्मनी में संघर्षों ने यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया। ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्गों ने अपनी शक्ति को केंद्रीकृत किया और सम्राट की सत्ता को स्थापित किया, जबकि रूस में पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट ने आधुनिक यूरोपीय शक्ति के रूप में रूस को स्थापित किया। जर्मनी में तीस वर्षीय युद्ध ने पवित्र रोमन साम्राज्य को कमजोर किया और राज्य की स्वायत्तता को बढ़ाया। कुल मिलाकर, यूरोप में पूर्ण राजशाही का विकास और जर्मनी में संघर्ष ने यूरोपीय राजनीति को नए मोड़ दिए और आधुनिक यूरोप की नींव रखी।
2-(C) Absolutism in Austria and Russia, Conflict in Germany.
Absolutism in Austria and Russia, and the Conflict in Germany
The rise of absolutism across Europe in the early modern period marked a significant shift in the balance of power within European states. Absolutism, in which monarchs held supreme authority over the state and its people, was a defining feature of the political landscape of many European nations during the 17th and 18th centuries. Austria and Russia, two of the great powers of Eastern Europe, were among the countries where absolutist monarchies flourished, while the German-speaking lands faced their own unique challenges and conflicts, primarily due to the complex political structure of the Holy Roman Empire. This essay will explore the development of absolutism in Austria and Russia, the challenges they faced, and the conflicts that characterized German-speaking lands in the early modern period, particularly focusing on the Thirty Years’ War.
Absolutism in Austria
The Rise of the Habsburg Dynasty
The history of absolutism in Austria is intricately tied to the power of the Habsburg dynasty, which ruled Austria and much of Central Europe for centuries. The Habsburgs first came to prominence in the 15th century and gradually expanded their power, inheriting various territories through dynastic marriages. By the 16th century, the Habsburgs had become one of the most powerful families in Europe, ruling over vast lands, including Austria, Bohemia, Hungary, and parts of Italy and the Low Countries.
Under the reign of Emperor Charles V (1519–1556), the Habsburg Empire was the largest and most powerful state in Europe. However, after his abdication, the empire was divided between his son, Philip II of Spain, and his brother, Ferdinand I, who became the Holy Roman Emperor and ruled over the Austrian lands. It was under Ferdinand’s descendants that Austria would begin its journey towards absolute monarchy.
The Establishment of Absolutism under the Habsburgs
The Habsburgs, particularly during the reign of Leopold I (1658–1705), began centralizing power and establishing absolutist rule in Austria. Leopold I was a key figure in the Habsburg struggle to maintain control over their diverse and often rebellious territories, including Hungary and Bohemia. To strengthen his power, Leopold sought to diminish the influence of the nobility and assert royal authority over the diverse regions within his empire. One of his key strategies was to assert control over the church, which had been a major source of power for the nobility.
The major events that shaped Austrian absolutism include the wars with the Ottoman Empire, which were crucial in defining the Habsburgs’ eastern borders and their central role in European politics. Leopold’s efforts to consolidate his power were furthered by his success in defending Austria from the Ottoman Empire at the Battle of Vienna (1683), where the Habsburgs, with the help of European allies, defeated the Ottomans and ended their threat to Central Europe.
The Treaty of Karlowitz (1699), which concluded the war with the Ottomans, further solidified Habsburg power and allowed Austria to expand its territory. This victory also enhanced the authority of the Habsburgs, contributing to the growth of absolutism. Over the next century, the Habsburg monarchy would continue to centralize its power, though Austria’s absolutism faced ongoing challenges from its diverse populations and external forces.
Maria Theresa and the Final Consolidation of Absolutism
The reign of Maria Theresa (1740–1780) represents the high point of Austrian absolutism. Maria Theresa inherited the throne during a period of political instability, following the War of Austrian Succession (1740–1748). To secure her reign, she worked to centralize the government and reduce the power of the nobility, an essential step in the consolidation of absolutism.
Maria Theresa implemented significant administrative and legal reforms. She reorganized the central government and reformed the military, which had suffered in the earlier conflicts. In addition to military reforms, she introduced economic policies that encouraged industry and improved the infrastructure of her empire. She also pursued religious policies that aimed to centralize control over the Catholic Church in her lands, reinforcing the authority of the crown over ecclesiastical matters.
Despite her efforts to strengthen the monarchy, Maria Theresa’s absolutist policies faced resistance from the nobility, particularly in Hungary, where they had long enjoyed significant autonomy. However, her son, Joseph II (reigned 1780–1790), went even further in implementing absolutist reforms. Joseph’s radical reforms, including attempts to reduce the power of the church and implement enlightened absolutism, would eventually lead to political and social unrest. His attempts to centralize power faced strong opposition, particularly from Hungary and the nobility, and many of his reforms were reversed after his death.
Absolutism in Russia
The Rise of the Romanov Dynasty
The history of absolutism in Russia is largely shaped by the Romanov dynasty, which ruled Russia from 1613 until the Russian Revolution in 1917. The Romanovs came to power following the Time of Troubles (1598–1613), a period of political instability and social upheaval. The establishment of the Romanov family as rulers of Russia provided stability, but it also set the stage for the centralization of power under the Russian monarchy.
Peter the Great and the Transformation of Russia
The most significant figure in the development of Russian absolutism was Peter the Great (reigned 1682–1725). Peter the Great sought to transform Russia into a modern European power, and his reign was marked by a series of radical reforms aimed at centralizing power and modernizing the country. He aimed to bring Russia in line with Western Europe, especially in terms of military and administrative structure.
Peter’s reforms focused on the military, where he introduced a modernized army and navy, allowing Russia to become a major military power in Europe. He also sought to reduce the power of the Russian nobility (the boyars) by introducing new administrative structures that concentrated power in the hands of the monarch. Peter implemented reforms to reduce the influence of the Russian Orthodox Church, thereby diminishing its authority and ensuring the monarchy’s supremacy in religious matters.
One of Peter’s most significant achievements was the establishment of St. Petersburg, a new capital city built on the Baltic Sea. This city symbolized Peter’s desire to create a “window to the West” and to transform Russia into a modern European state. Through his reforms, Peter created a powerful centralized state and solidified the idea of absolute monarchy in Russia.
Catherine the Great and Continued Centralization
Catherine the Great (reigned 1762–1796) continued the work of Peter the Great, further centralizing power and expanding the Russian Empire. Catherine was an enlightened monarch who implemented a number of reforms, but like Peter, she was ultimately an absolutist ruler. She expanded the Russian Empire through military campaigns, including the partitions of Poland, which significantly increased Russian territory.
Catherine’s reign is often associated with the “Golden Age” of the Russian nobility, as she relied on the support of the aristocracy to maintain her power. Despite her enlightened ideas, Catherine was unwilling to challenge the entrenched system of serfdom, which remained widespread in Russia. The growth of serfdom during her reign led to increased social tensions, particularly among the peasantry, and would remain a key issue in Russian politics for many years.
Conflict in Germany: The Thirty Years’ War
The Holy Roman Empire and the Rise of Religious Tensions
The political structure of Germany during the early modern period was extremely fragmented. The Holy Roman Empire, which covered much of modern-day Germany, was a complex collection of semi-autonomous territories under the nominal rule of the emperor. The emperor’s power was limited, and the individual princes and electors held significant control over their territories. This decentralized structure made it difficult to establish a unified state in Germany.
The Thirty Years’ War (1618–1648) was one of the most devastating conflicts in European history and had a profound impact on the German-speaking lands. The war was sparked by religious tensions between Protestant and Catholic states within the Holy Roman Empire, following the Protestant Reformation. It began as a struggle between Catholic Habsburg rulers and Protestant states, but it quickly escalated into a broader European conflict, involving France, Sweden, and other powers.
The Devastation of the Thirty Years’ War
The war had devastating consequences for Germany. It resulted in widespread destruction, particularly in the northern and central regions of the Holy Roman Empire. The conflict led to the deaths of millions of people, either through battle, famine, or disease. The war also significantly weakened the power of the Holy Roman Empire, as the peace settlements that followed, particularly the Peace of Westphalia (1648), recognized the independence of many of the German states.
The war also exacerbated the religious divide in the Holy Roman Empire, with Catholic and Protestant factions further entrenched in their positions. The Peace of Westphalia established a new political order in Germany, with greater autonomy for the individual German states, and marked the end of large-scale religious conflicts within the Holy Roman Empire. However, the division between Catholic and Protestant states in Germany would persist for centuries, and the fragmented political landscape would continue to make it difficult for Germany to unify under a single monarch.
Conclusion
Absolutism in Austria and Russia and the conflicts in Germany during the early modern period were critical in shaping the political and social structures of Eastern Europe. In Austria, the Habsburgs successfully established a powerful absolutist monarchy, although they faced challenges in their diverse empire. In Russia, Peter the Great and Catherine the Great were instrumental in transforming Russia into a centralized, absolutist state. Meanwhile, the fragmented nature of Germany, coupled with the religious and political turmoil of the Thirty Years’ War, hindered the development of absolutism in the German-speaking lands. Ultimately, the development of absolutism in Europe was shaped by the actions of powerful monarchs and the conflicts that defined the era.
2-(D) The Emergence of the Nation-State in Europe.
यूरोप में राष्ट्र-राज्य का उदय
यूरोप में राष्ट्र-राज्य का उदय महाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यह प्रक्रिया, जो कई सदियों तक चली, आधुनिक राज्यों के विकास की ओर ले गई जो एक परिभाषित भूभाग, एक केंद्रीय सरकार और एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में पहचाने जाते हैं। मध्यकालीन राजतंत्रों और बिखरे साम्राज्यों से लेकर आधुनिक राष्ट्र-राज्य के निर्माण तक की यह यात्रा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ-साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और विचारकों के प्रभाव से प्रेरित थी। इस निबंध में, हम यूरोप में राष्ट्र-राज्य के उदय, इसके उत्पत्ति, विकास, प्रमुख घटनाओं और उन कारकों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया।
I. मध्यकालीन काल और संप्रभुता की अवधारणा
जिस राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को हम आज समझते हैं, वह मध्यकालीन काल में अस्तित्व में नहीं था। इसके बजाय, यूरोप विभिन्न राज्यों, साम्राज्य और नगर-राज्यों के बीच बंटा हुआ था। मध्यकालीन राजनीतिक प्रणाली भूमि के मालिकों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर आधारित थी, जिन्हें सामंती व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें स्थानीय प्रभुओं को अपनी क्षेत्रों पर काफी अधिकार प्राप्त थे। सम्राटों के पास सर्वोच्च सत्ता थी, लेकिन वे अक्सर अपने अधीनस्थों के नियंत्रण में होते थे, जिनके पास स्वतंत्रता होती थी।
प्रारंभिक मध्यकाल में, यूरोप कई साम्राज्यों का घर था, जिनमें सबसे प्रमुख था पवित्र रोमन साम्राज्य, जो यूरोप के बड़े हिस्से को एकीकृत करने का प्रयास करता था। हालांकि, सम्राट की शक्ति साम्राज्य की विकेंद्रीकृत संरचना द्वारा सीमित थी, और स्थानीय शासक अक्सर सम्राट के अधिकारों से स्वतंत्र रहते थे।
फिर भी, मध्यकाल के अंत में संप्रभुता—जो एक शासक के द्वारा परिभाषित भूभाग पर सर्वोच्च अधिकार की अवधारणा है—की कल्पना बनने लगी थी। सामंती व्यवस्था का पतन, शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय और अधिक केंद्रीकृत सरकारों का निर्माण आधुनिक राष्ट्र-राज्य के गठन के लिए नींव रख रहा था।
II. शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय
राष्ट्र-राज्य के उदय में एक महत्वपूर्ण योगदान देर मध्यकाल में शक्तिशाली राजतंत्रों का गठन था। राजाओं द्वारा सत्ता के केंद्रीकरण ने उन्हें कानून लागू करने, कर इकट्ठा करने और स्थायी सेनाओं को बनाए रखने में सक्षम बनाया। यह केंद्रीकृत शासन की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति विशेष रूप से फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन में स्पष्ट रूप से देखी गई, जहां शासकों ने अपनी भूमि को एकीकृत करने और सामंती प्रभुओं की शक्ति को कम करने का प्रयास किया।
फ्रांस में, सौ साल का युद्ध (1337–1453) फ्रांसीसी राष्ट्र-राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध न केवल फ्रांसीसी लोगों के बीच एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने में मदद करता है, बल्कि शाही शक्ति के केंद्रीकरण में भी योगदान करता है। फ्रांसीसी राजतंत्र ने अपने अधिकार को एकजुट किया, सामंती प्रभुओं का प्रभाव कम किया, और एक मजबूत, केंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया।
इंग्लैंड में, राष्ट्र-राज्य का विकास घटनाओं जैसे नॉर्मन आक्रमण (1066), मैग्ना कार्टा का हस्ताक्षर (1215) और अंग्रेजी गृहयुद्ध (1642–1651) से प्रभावित था। नॉर्मन आक्रमण ने इंग्लैंड में केंद्रीकृत शाही अधिकार लाया, और मैग्ना कार्टा ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सम्राट का अधिकार कानून से सीमित था। अंग्रेजी गृहयुद्ध, जिसने किंग चार्ल्स I की फांसी और ओलिवर क्रॉमवेल के तहत राष्ट्रगणराज्य की स्थापना की, ने संविधानात्मक राजतंत्र और आधुनिक राष्ट्र-राज्य के विकास में योगदान किया।
स्पेन में, कैथोलिक सम्राटों, फर्डिनेंड और इसाबेला के तहत, 15वीं शताब्दी में इबेरियन प्रायद्वीप का एकीकरण हुआ। उनका विवाह, जिसने अरागॉन और कास्टिले के राज्यों को जोड़ा, स्पेन के राष्ट्र-राज्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम था। रिकांquista, मुस्लिमों को स्पेन से बाहर निकालने का प्रयास, एक एकीकृत स्पेनिश पहचान के निर्माण में भी भूमिका निभाई।
III. पुनर्जागरण और मानवतावाद का प्रभाव
पुनर्जागरण (14वीं–17वीं शताब्दी) एक ऐसा काल था जिसमें बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पुनःउत्थान हुआ और इसका राष्ट्र-राज्य के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण में प्राचीन काल के विचारों की ओर पुनः रूचि जागी, जिसने शासन, व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की भूमिका के बारे में नए विचारों को जन्म दिया। मानवतावादी विचारकों, जैसे निकोलो माचियावेली ने राजनीतिक शक्ति और संप्रभुता की प्रकृति के बारे में सिद्धांत विकसित किए, जिन्होंने आधुनिक राष्ट्र-राज्य के निर्माण में प्रभाव डाला।
माचियावेली का कार्य “द प्रिंस” (1513) पुनर्जागरण राजनीतिक विचारों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस ग्रंथ में माचियावेली ने तर्क किया कि शासकों को अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके से, जिसमें बल और धोखा शामिल हो, सशक्त होना चाहिए। यह शासन की यह दृष्टि एक मजबूत, केंद्रीकृत राज्य के महत्व को रेखांकित करती है, जो यूरोप में बढ़ती हुई पूर्ण राजशाही के रुझानों से मेल खाती थी।
पुनर्जागरण ने राष्ट्रीयता के विकास में भी योगदान दिया, क्योंकि इसने एकजुट राष्ट्रीय संस्कृति के विचार को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय भाषाओं, साहित्य और कला का विकास ने विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के लोगों के बीच पहचान और संबंध की भावना को बढ़ावा दिया। यह सांस्कृतिक एकता आधुनिक राष्ट्र-राज्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसने साझा इतिहास और धरोहर की भावना को जन्म दिया, जिसका बाद में राज्य की वैधता को सही ठहराने के लिए उपयोग किया गया।
IV. सुधार और धार्मिक संघर्ष
प्रोटेस्टेंट सुधार (1517–1648) का यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा और राष्ट्र-राज्य के निर्माण में योगदान किया। सुधार, जो मार्टिन लूथर द्वारा 95 थिसिस (1517) के माध्यम से शुरू हुआ था, ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी और प्रोटेस्टेंट सम्प्रदायों की नींव रखी। सुधार से उत्पन्न धार्मिक विभाजन राष्ट्र-राज्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक बन गए, क्योंकि शासकों ने अपने क्षेत्रों में धार्मिक मामलों पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया।
देशों जैसे इंग्लैंड में, सुधार ने एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पोप से अलग था। हेनरी VIII द्वारा 1530 के दशक में चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना ने शाही शक्ति के केंद्रीकरण में योगदान किया और इंग्लिश राष्ट्र-राज्य के निर्माण को सुदृढ़ किया।
रूढ़िवादी और प्रोटेस्टेंट के बीच धार्मिक युद्धों, जैसे तीस वर्षीय युद्ध (1618–1648) ने भी राष्ट्र-राज्य के विकास में योगदान किया। वेस्टफालिया की संधि, जिसने तीस वर्षीय युद्ध को समाप्त किया, ने “कुईउस रेजियो, ईउस रिलिजियो” (जिसका अर्थ है, जिस राज्य का शासक, उसी का धर्म) के सिद्धांत को मान्यता दी। इस सिद्धांत ने शासकों के अधिकार को मजबूत किया और राष्ट्र-राज्य के सिद्धांत को बढ़ावा दिया।
V. अन्वेषण युग और वैश्विक साम्राज्यों का उदय
अन्वेषण युग (15वीं–17वीं शताब्दी) ने यूरोप में राष्ट्र-राज्य के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। यूरोपीय देशों जैसे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड ने समुद्री रास्तों की खोज की और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश स्थापित किए, जिससे न केवल उनके आर्थिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई बल्कि राष्ट्रीय पहचान का भी विकास हुआ। इन उपनिवेशों ने यूरोपीय शासकों के लिए एक केंद्रीकृत राज्य बनाने में सहायता की और इसने मजबूत केंद्रीय राज्यों के निर्माण को बढ़ावा दिया।
वैश्विक व्यापार का उदय, जो यूरोपीय अन्वेषण से प्रेरित था, ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास और राष्ट्र-राज्य के सुदृढ़ीकरण में योगदान किया। विदेशी व्यापार से प्राप्त धन ने यूरोपीय सम्राटों को मजबूत केंद्रीकृत राज्य बनाने में सहायता की, जिससे वे स्थायी सेनाओं को बनाए रख सके, बुनियादी ढांचे का विकास कर सके, और अपने क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित कर सके।
यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार ने वैश्विक कूटनीति के एक प्रणाली की नींव भी रखी, जिसमें राष्ट्र-राज्य आपस में गठबंधन, व्यापार समझौते और संघर्षों को हल करने के लिए बातचीत करते थे। इस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ने राष्ट्र-राज्य के सिद्धांत को और सुदृढ़ किया और वैश्विक राजनीति में राष्ट्र-राज्य को केंद्रीय भूमिका के रूप में स्थापित किया।
VI. युग of उन्नति और राष्ट्र-राज्य का सिद्धांत
उन्नति युग (17वीं–18वीं शताब्दी) बौद्धिक विकास का एक युग था जिसमें तर्क, व्यक्तिगत अधिकारों और शासन के प्रकार पर विचार किया गया। उन्नति विचारक जैसे जॉन लॉक, जीन-जैक्स रूसो और मोंटेस्क्यू ने राज्य की प्रकृति और शासक और नागरिकों के बीच संबंधों के बारे में नए विचार विकसित किए। इन विचारों ने राष्ट्र-राज्य के विकास में गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि इन्होंने राज्य शक्ति की वैधता के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया।
जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के विचारों ने लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य के विकास को आकार देने में मदद की। लॉक का मानना था कि व्यक्तियों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार होते हैं और सरकार का उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना होता है। रूसो ने “सामाजिक अनुबंध” (1762) में तर्क किया कि वै
ध राजनीतिक अधिकार केवल शासितों की सहमति से उत्पन्न होते हैं। इन विचारों ने पूर्ण राजतंत्र के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी और यूरोप में संविधानात्मक राजतंत्र और गणराज्य के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया।
VII. फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक राष्ट्रीयता का जन्म
फ्रांसीसी क्रांति (1789–1799) राष्ट्र-राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस क्रांति ने फ्रांस में पूर्ण राजशाही का अंत किया और गणराज्य की स्थापना की। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचार फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान का केंद्रीय हिस्सा बन गए, और इस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया।
फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय को भी चिह्नित किया। यह विचार कि जो लोग एक सामान्य भाषा, संस्कृति और इतिहास साझा करते हैं, उन्हें अपना राज्य होना चाहिए, यूरोप में एक शक्तिशाली बल बन गया। फ्रांसीसी क्रांति, साथ ही नेपोलियन युद्धों ने यूरोप भर में राष्ट्रवादी विचारों को फैलाया और 19वीं शताब्दी में राष्ट्र-राज्य के निर्माण के लिए नींव रखी।
VIII. निष्कर्ष
यूरोप में राष्ट्र-राज्य का उदय एक जटिल प्रक्रिया थी, जो कई सदियों तक चली और इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय, पुनर्जागरण और सुधार का प्रभाव, यूरोपीय साम्राज्यों का विस्तार, और उन्नति के विचार ने राष्ट्र-राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय ने राष्ट्र-राज्य के सिद्धांत को और मजबूत किया, जो यूरोप और अंततः दुनिया में राजनीतिक संगठन का मुख्य रूप बन गया। राष्ट्र-राज्य का उदय यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की नींव रखी।
2-(D) The Emergence of the Nation-State in Europe.
The Emergence of the Nation-State in Europe
The emergence of the nation-state in Europe was one of the most significant transformations in the political landscape of the continent. This process, which took several centuries, resulted in the development of modern states that are characterized by a defined territory, a central government, and a sense of national identity. The evolution from medieval kingdoms and fragmented empires to the modern nation-state involved a variety of political, social, economic, and cultural changes, as well as the influence of major historical events and thinkers. In this essay, we will explore the emergence of the nation-state in Europe, focusing on its origins, development, key events, and the factors that contributed to its formation.
I. The Medieval Period and the Concept of Sovereignty
The concept of the nation-state, as we understand it today, did not exist during the medieval period. Instead, Europe was dominated by a patchwork of kingdoms, principalities, and city-states. The medieval political system was based on feudalism, a decentralized form of governance in which local lords had significant power over their territories. Monarchs, while recognized as the supreme rulers, often struggled to control their vassals, who held significant autonomy.
During the early medieval period, Europe was also home to a number of empires, most notably the Holy Roman Empire, which sought to unify large parts of Europe under a single political entity. However, the power of the emperor was limited by the decentralized structure of the empire, and local rulers often acted independently of imperial authority.
Despite the lack of centralized control, the idea of sovereignty—defined as the supreme authority of a ruler over a defined territory—began to take shape during the late Middle Ages. The decline of feudalism, the rise of powerful monarchies, and the emergence of more centralized governments laid the groundwork for the formation of modern nation-states.
II. The Rise of Strong Monarchies
A key factor in the emergence of the nation-state was the rise of powerful monarchies in the late Middle Ages. The consolidation of power by monarchs allowed them to create centralized states that were capable of enforcing laws, collecting taxes, and maintaining standing armies. This shift toward centralized rule was particularly evident in France, England, and Spain, where monarchs sought to unify their territories and reduce the power of the nobility.
In France, the Hundred Years’ War (1337–1453) played a pivotal role in the development of the French nation-state. The war between England and France not only helped to forge a sense of national identity among the French people but also led to the centralization of royal power. The French monarchy, under leaders like Charles VII, successfully consolidated authority, diminished the influence of feudal lords, and built a strong, centralized state.
In England, the development of the nation-state was influenced by events such as the Norman Conquest (1066), the signing of the Magna Carta (1215), and the English Civil War (1642–1651). The Norman Conquest brought centralized royal authority to England, and the Magna Carta established the principle that the monarch’s power was limited by law. The English Civil War, which culminated in the execution of King Charles I and the establishment of the Commonwealth under Oliver Cromwell, further contributed to the development of constitutional monarchy and the rise of the modern nation-state.
Spain, under the Catholic Monarchs Ferdinand and Isabella, achieved the unification of the Iberian Peninsula in the late 15th century. Their marriage, which united the kingdoms of Aragon and Castile, was a crucial step in the formation of the Spanish nation-state. The Reconquista, the effort to expel the Moors from Spain, also played a role in the creation of a unified Spanish identity.
III. The Impact of the Renaissance and Humanism
The Renaissance (14th–17th centuries) was a period of intellectual, cultural, and artistic revival that had a profound impact on the development of the nation-state. The Renaissance saw a renewed interest in classical antiquity, which inspired new ideas about governance, individual rights, and the role of the state. Humanist thinkers, such as Niccolò Machiavelli, began to develop theories about political power and the nature of sovereignty that would influence the formation of the modern nation-state.
Machiavelli’s work “The Prince” (1513) is one of the most significant examples of Renaissance political thought. In this treatise, Machiavelli argued that rulers should be pragmatic and willing to do whatever necessary to maintain power, including the use of force and deceit. This approach to governance emphasized the importance of a strong, centralized state led by a powerful ruler—an idea that resonated with the growing trend of absolute monarchy in Europe.
The Renaissance also contributed to the rise of nationalism by promoting the idea of a unified national culture. The development of national languages, literature, and art helped to foster a sense of identity and belonging among the people of different European nations. This cultural unification was an important step toward the formation of modern nation-states, as it created a shared sense of heritage and history that would later be used to justify the legitimacy of the state.
IV. The Reformation and Religious Conflict
The Protestant Reformation (1517–1648) had a profound effect on the political landscape of Europe and contributed to the formation of nation-states. The Reformation, initiated by Martin Luther’s 95 Theses in 1517, challenged the authority of the Catholic Church and led to the creation of Protestant denominations. The religious divisions that resulted from the Reformation were a major factor in the formation of nation-states, as rulers sought to assert their authority over religious matters within their territories.
In countries such as England, the Reformation played a crucial role in the establishment of a national church that was separate from the papacy. Henry VIII’s establishment of the Church of England in the 1530s was a key moment in the consolidation of royal power and the development of the English nation-state. The English monarchy’s control over religious matters further centralized power in the hands of the king, reinforcing the idea of a unified national identity.
The religious wars that followed the Reformation, including the Thirty Years’ War (1618–1648), also played a role in the development of nation-states. The Treaty of Westphalia, which ended the Thirty Years’ War, recognized the principle of cuius regio, eius religio—meaning that the ruler of a territory could determine the religion of its subjects. This principle helped to solidify the authority of rulers over their territories and contributed to the formation of modern nation-states by reinforcing the idea of state sovereignty.
V. The Age of Exploration and the Rise of Global Empires
The Age of Exploration (15th–17th centuries) had a profound impact on the development of the nation-state in Europe. European nations, such as Spain, Portugal, France, and England, began to establish overseas empires, which not only expanded their economic and military power but also fostered the growth of national identities. The establishment of colonies in the Americas, Africa, and Asia helped to consolidate the power of European monarchs and encouraged the formation of more centralized states.
The rise of global trade, facilitated by European exploration, also contributed to the development of the modern economy and the strengthening of the nation-state. The wealth generated by overseas trade allowed European monarchs to build strong centralized states with the resources to maintain standing armies, develop infrastructure, and control their territories more effectively.
The expansion of European empires also led to the establishment of a global system of diplomacy, in which nation-states interacted with one another to form alliances, negotiate trade agreements, and resolve conflicts. This system of international relations further reinforced the idea of the nation-state as a central actor in global politics.
VI. The Enlightenment and the Theory of the Nation-State
The Enlightenment (17th–18th centuries) was a period of intellectual growth that focused on reason, individual rights, and the role of government. Enlightenment thinkers, such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau, and Montesquieu, developed new ideas about the nature of the state and the relationship between rulers and citizens. These ideas would have a profound impact on the development of modern nation-states, as they provided a theoretical foundation for the legitimacy of state power.
John Locke’s ideas about natural rights and the social contract helped to shape the development of democratic nation-states. Locke argued that individuals had certain inalienable rights, such as life, liberty, and property, and that governments were created to protect these rights. Rousseau, in his work “The Social Contract” (1762), argued that legitimate political authority comes from the consent of the governed. These ideas challenged the traditional notions of absolute monarchy and helped to pave the way for the development of constitutional monarchies and republics in Europe.
VII. The French Revolution and the Birth of Modern Nationalism
The French Revolution (1789–1799) was a pivotal moment in the development of the modern nation-state. The revolution brought about the end of absolute monarchy in France and the establishment of a republic. The ideas of liberty, equality, and fraternity became central to the French national identity, and the revolution inspired movements for national self-determination across Europe.
The French Revolution also marked the rise of modern nationalism. The idea that people who shared a common language, culture, and history should have their own state became a powerful force in Europe. The French Revolution, along with the Napoleonic Wars, spread nationalist ideals throughout Europe and laid the groundwork for the creation of nation-states in the 19th century.
VIII. Conclusion
The emergence of the nation-state in Europe was a complex process that spanned several centuries and was influenced by a variety of political, social, economic, and cultural factors. The rise of powerful monarchies, the impact of the Renaissance and Reformation, the expansion of European empires, and the ideas of the Enlightenment all played crucial roles in the development of the modern nation-state. The French Revolution and the rise of nationalism in the 19th century further solidified the concept of the nation-state, which became the dominant form of political organization in Europe and, eventually, the world. The emergence of the nation-state fundamentally changed the political landscape of Europe and laid the foundation for the modern international system.